अध्याय-3 कर्मयोग
अर्जुन ने कहा, “हे जनार्दन, हे केशव! यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके व्यंग्य मिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। अतः कृपा करके निश्चयपूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा।”
श्री भगवान ने कहा, “हे निष्पाप अर्जुन! मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्मसाक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा।
ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षणभर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता।
जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह उत्कृष्ट है।
इसलिए अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंतीपुत्र! उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे।
सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, ‘तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी।’
यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है।
भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग, जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है।
वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और यह वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हे प्रिय अर्जुन! जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है।
किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्मसाक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं होता। क्योंकि उस व्यक्ति को ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती।
अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पारब्रह्म की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए।
महापुरुष जो-जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है।
हे पृथापुत्र! तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानीपूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ! यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे।
यदि मैं नियत कर्म ना करूं, तो यह सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जनसमुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा।”
जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हों। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो।
जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे महाबाहो! भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली-भांति जानते हुए, जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता।
माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके यह कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें।
अतः हे अर्जुन! अपने सारे कार्यों को मुझमें समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो।
जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार आचरण करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्या वश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट-भ्रष्ट समझना चाहिए।
ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग-द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्मसाक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं।
अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली-भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वकर्मों को करते हुए मरना, पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है।
अर्जुन ने कहा, “हे वृष्णवंशी! मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो।”
श्री भगवान ने कहा, “हे अर्जुन! इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है।
जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है।
इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन! प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मसाक्षात्कार के इस विनाशक का वध करो।
कर्म इंद्रिय जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है।
इस प्रकार, हे महाबाहु अर्जुन! अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो।”
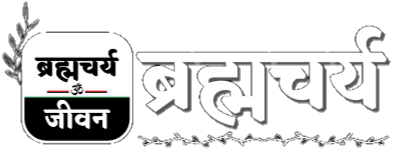
Leave a comment