अध्याय-2 गीता का सार
संजय ने कहा – करुणा से व्याप्त, शोकयुक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे।
श्री भगवान ने कहा –
हे अर्जुन! तुम्हारे मन में यह कल्मष आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं, अपितु अपयश की प्राप्ति होती है।
हे प्रथापुत्र! इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमनकर्ता! हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो।
अर्जुन ने कहा –
हे शत्रुहंता! हे मधुसूदन! मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा?
ऐसे महापुरुषों को, जो मेरे गुरु हैं, मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी।
हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है – उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं।
अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। कृपया मुझे उपदेश दें।
मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता, जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन-धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा।
संजय ने कहा –
इस प्रकार कहने के बाद, शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला – “हे गोविंद! मैं युद्ध नहीं करूंगा।” और चुप हो गया।
हे भरतवंशी धृतराष्ट्र! उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे।
श्री भगवान ने कहा –
तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो, जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं, वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा यह समस्त राजा न रहे हों। और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे।
जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीरवान व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता।
हे कुंतीपुत्र! सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतरध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने-जाने के समान है। हे भरतवंशी! वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे।
हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन! जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है।
तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तनीय रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है।
जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है।
अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी! युद्ध करो।
जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं; क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है।
आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता।
हे पार्थ! जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है?
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है।
यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड-खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है।
यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक-सा रहने वाला है।
यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए।
किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु! तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है।
जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।
सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है?
कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। किंतु कोई-कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं।
हे भरतवंशी! शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है।
क्षत्रिय होने के नाते, अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हे पार्थ! वे क्षत्रिय सुखी हैं, जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं।
किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे।
लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन-जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे।
तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है?
हे कुंतीपुत्र! तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो।
तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा।
यहां मैंने वैशेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र! तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो।
इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही रास। अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है।
हे कुरुनंदन! जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है।
अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं – इससे बढ़कर और कुछ नहीं है।
जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता।
वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन! इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो।
एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार, वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं।
तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो।
हे अर्जुन! जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है।
हे धनंजय! भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे कृपण हैं।
भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य-कौशल यही है।
इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े-बड़े ऋषि-मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म-मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, जो समस्त दुखों से परे है।
जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमस्त हो जाओगे।
जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्मसाक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी।
अर्जुन ने कहा –
हे कृष्ण! अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है?
श्री भगवान ने कहा –
हे पार्थ! जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थितप्रज्ञ कहा जाता है।
जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है।
इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है।
जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है।
देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से, ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है।
हे अर्जुन! इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है।
जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है।
इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है।
क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है।
किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है।
इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है।
जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है?
जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है।
अतः हे महाबाहु! जिस पुरुष की इंद्रियां अपने-अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है।
जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है।
जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं, जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो।
जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है।
यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवद्धाम में प्रवेश कर सकता है।
।।बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।।
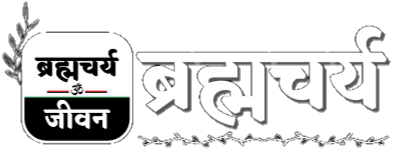
Leave a comment